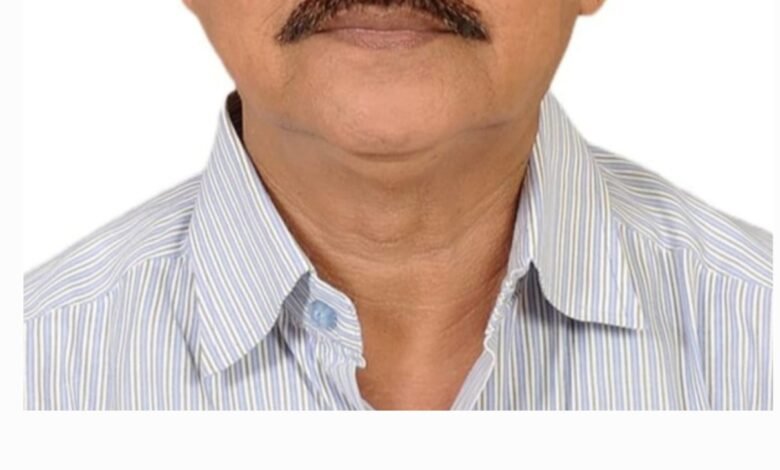
जनपथ न्यूज़जि
तेन्द्र कुमार सिन्हा, पटनारा
राजनीति को समाज के संचालन की रीढ़ माना गया है। लोकतंत्र का ताना-बाना राजनीति से ही बुना जाता है। लेकिन राजनीति और लोकतंत्र का संबंध वैसा ही है जैसा आत्मा और शरीर का, जब राजनीति में ईमानदारी, त्याग और सेवा की भावना प्रबल होती है, तब लोकतंत्र सशक्त और जीवंत दिखाई देता है और जब राजनीति केवल सत्ता-लोलुपता, छल-प्रपंच और भ्रष्टाचार का माध्यम बन जाता है, तब लोकतंत्र खोखला और बेमानी प्रतीत होने लगता है। आज की स्थिति में यही संकट भारतीय लोकतंत्र, विशेषकर बिहार की राजनीति पर गहराई से हावी है। चुनावी मौसम आते ही संवैधानिक संस्थाएँ, न्यायपालिका और कार्यपालिका का स्वरूप भी सवालों के घेरे में आ जाता है।

लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ ऐसा स्वर्णिम पल रहा है जब राजनीति और संवैधानिक संस्थाओं का संतुलन आदर्श रूप में दिखता था। टी.एन. शेषन (भारत के दसवें मुख्य चुनाव आयुक्त) ने चुनाव आयोग को जिस मजबूती और गरिमा से खड़ा किया था, वह लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर है। उनके कठोर कदमों ने दिखाया था कि यदि ईमानदार और निडर अफसरशाही सत्ता के दबाव से ऊपर उठकर काम करे तो चुनाव वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सकता है। चंद्रशेखर, पी.वी. नरसिंहा राव और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे राजनेता लोकतांत्रिक मर्यादाओं के प्रतीक थे। इन नेताओं ने न केवल सत्ता चलाई बल्कि विरोधियों का सम्मान भी किया। संसद की गरिमा बनी रही और संस्थाओं के प्रति विश्वास कायम रहा। यह वह दौर था जब राजनीति सत्ता प्राप्ति का साधन जरूर था, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा, संवाद, मर्यादा और पारदर्शिता जीवित थी।

आज की राजनीति में तस्वीर बिल्कुल उलटी है। बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष और आयोग के बीच जो टकराव सामने आ रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग अब वह स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था नहीं रहा जो कभी टी.एन. शेषन के दौर में था। आयोग पर राजनीतिक दबाव और सत्ता के हित साधने के आरोप लग रहे हैं। लोकतंत्र की अंतिम आस होती है न्यायपालिका। लेकिन यदि चुनावी प्रक्रिया, परिणामों और राजनीतिक दांव-पेंचों में न्यायपालिका को बार-बार घसीटा जाए तो उसकी निष्पक्षता और गरिमा पर भी प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। अफसरशाही, जो कभी शासन संचालन का मेरुदंड हुआ करती थी, अब राजनीतिक स्वार्थ की कठपुतली जैसी दिख रही है। अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से अधिक राजनीतिक आकाओं की सेवा में लिप्त रहते हैं। इससे आम जन की समस्याएँ बढ़ती हैं।

बिहार का राजनीतिक परिदृश्य हमेशा से अनोखा और जटिल रहा है। जातीय समीकरण, गठबंधन की राजनीति और परिवारवाद ने यहां लोकतंत्र को एक विशेष ढांचा दिया है। इस बार की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगियों की एनडीए बनाम महागठबंधन (राजद, कांग्रेस एव अन्य) के बीच है। राजद का कैडर वोट अब भी मजबूत दिखाई देता है। लालू यादव का करिश्मा और सामाजिक न्याय का नारा अब भी प्रभावी है। भाजपा अपने संगठन और हिंदुत्व-राष्ट्रवाद की रणनीति के सहारे मैदान में है। कांग्रेस अपनी खोई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। जनता दल यूनाइटेड से अलग होने के बाद जन स्वराज पार्टी (पीके) अपने संगठनात्मक मॉडल के सहारे मैदान में हैं। लेकिन फिलहाल उनकी ताकत वोट-कटवा की ज्यादा प्रतीत हो रही है।
अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जनता बेहद परेशान है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली आम जन के लिए बड़ा संकट है। बाढ़ और प्रवासी मजदूरों की समस्या चुनावी विमर्श का हिस्सा बन सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार चुनाव में उतरने वाले केंद्रीय विपक्ष के पास एक मात्र यही हथियार है कि वे चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाएं। ऑपरेशन सिंदूर, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था जैसे राष्ट्रीय विमर्श से ध्यान हटाने के लिए विपक्ष आयोग को निशाने पर लेकर चल रहा है। यह रणनीति अल्पकालिक राजनीतिक लाभ दे सकता है, लेकिन दीर्घकाल में लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होगी। क्योंकि यदि जनता का भरोसा चुनाव आयोग जैसी संस्था पर से उठ जाएगा, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही बेमानी हो जाएगी।
बिहार के आम नागरिक की सबसे बड़ी चिंता अपराध, भ्रष्टाचार और व्यवस्था का अभाव है। बिहार लंबे समय से अपराध और राजनीतिक अपराधियों की शरणस्थली रहा है। आज भी अपहरण, हत्या, रंगदारी और बलात्कार जैसी घटनाएँ आम हैं। प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार इस कदर गहराया हुआ है कि लगता है बिना घूस दिए कोई काम पूरा नहीं होता है। शिक्षा व्यवस्था जर्जर है। सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं और रोजगार के अवसर न्यूनतम हैं। इन गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय यदि राजनीतिक दल सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप-प्रत्यारोप में उलझे रहेंगे, तो जनता का गुस्सा निश्चित ही और बढ़ेगा।
यदि राजनीति और संवैधानिक संस्थाएँ इसी राह पर चलती रही तो आने वाले समय में कुछ खतरनाक परिणाम सामने आ सकता है, जैसे- न्यायपालिका की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। कार्यपालिका अपनी स्वतंत्रता खो देगी। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल हमेशा बना रहेगा। जनता का लोकतंत्र पर विश्वास डगमगा जाएगा। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र केवल चुनाव तक सिमट जाएगा और उसका असली अर्थ “जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन” खत्म हो जाएगा।
आयोग को राजनीतिक दबाव से मुक्त करना आवश्यक है। नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और सर्वसम्मति आधारित बनाया जाना चाहिए। न्यायिक नियुक्तियों और फैसलों पर राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त होना चाहिए। राजनीति को सेवा और जनहित का माध्यम बनाना होगा। दलों को अपराधियों को टिकट देने से रोकने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। जनता को केवल जातीय समीकरण या चुनावी घोषणाओं के आधार पर वोट न देकर असली मुद्दों पर नेताओं से सवाल पूछना चाहिए।
आज की स्थिति में बिहार चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता की कसौटी भी है। यदि राजनीतिक दल केवल आयोग और न्यायपालिका पर हमला कर खुद को बचाते रहे और जनता की वास्तविक समस्याओं से मुंह मोड़ते रहे, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत होगा। राजनीति और राजनेता ऐसा वर्ग है जिनसे समाज के हर तबके को प्रेरणा और समाधान मिलना चाहिए। लेकिन यदि राजनीति ही अविश्वास, भ्रष्टाचार और अपराध का प्रतीक बन जाए तो लोकतंत्र की आत्मा मर जाएगी। यही कारण है कि आज सबसे बड़ी जरूरत है राजनीति में मर्यादा, संवैधानिक संस्थाओं में स्वतंत्रता और जनता में जागरूकता।
———–
![]()




